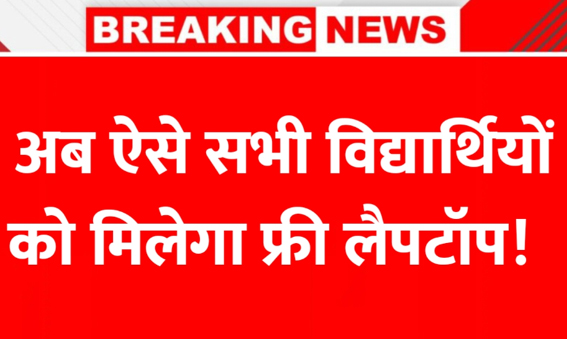बृज खंडेलवाल
कुछ तो हुआ है कि वॉशिंगटन के गलियारों में बेचैनी बढ़ गई है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अमेरिका का चेहरा तमतमा गया है, और ट्रंप का गुस्सा बयानों में झलक रहा है। ट्रंप दावा कर रहे हैं कि उन्होंने युद्धविराम कराया, लेकिन हकीकत यह है कि भारत पर दबाव बनाने के लिए टैरिफ हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। अंतरराष्ट्रीय सूत्र कहते हैं कि ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी से कई बार फोन पर बात करने की कोशिश की, मगर सफलता नहीं मिली। सैन्य विश्लेषकों का अनुमान है कि पाकिस्तान के परमाणु बंकरों को गहरा नुकसान पहुंचा है और कुछ अमेरिकी सैनिक भी मारे गए। ट्रंप भले ही सात फाइटर जेट ध्वस्त होने की बात कहें, लेकिन यह साफ है कि भारत की सैन्य कार्रवाई ने कहीं न कहीं अमेरिकी प्रतिष्ठा को चोट पहुंचाई है। रूस से तेल खरीद तो एक बहाना है, असली वजह है पाकिस्तान के ध्वस्त सैन्य ठिकाने और अमेरिका की कूटनीतिक हार।
गुस्से में आकर ट्रंप ने भारत का अपमान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जवाब में मोदी सरकार ने चुप्पी साधकर अमेरिकी बड़बोलेपन को चुनौती दी। यह मौन रणनीति है या विवशता, यह आने वाला समय ही बताएगा। मगर इस टकराव के बीच भारत जिस गंभीर स्थिति में आ गया है, वह किसी भी तरह अनदेखी नहीं की जा सकती। अमेरिका ने अपनी व्यापार नीति को भारत के लिए संकट बना दिया है। रूस से ऊर्जा और रक्षा सौदों को लेकर असहमति जताते हुए वॉशिंगटन ने भारत के 86.5 अरब डॉलर के निर्यात पर औसतन 50 प्रतिशत तक टैरिफ लगा दिया है। इसका सीधा असर उन उद्योगों पर पड़ा है जो भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाते हैं—हीरे-जवाहरात, परिधान, झींगा और रसायन। अनुमान है कि लगभग 60 अरब डॉलर का निर्यात मूल्य सीधे-सीधे प्रभावित होगा।
सबसे बड़ी चोट छोटे और मझोले उद्योगों पर पड़ी है। सूरत का हीरा उद्योग और तिरुपुर का वस्त्र निर्यात पहले ही वैश्विक मंदी और मुद्रा उतार-चढ़ाव की मार झेल रहा था, अब अमेरिकी टैरिफ ने उनकी प्रतिस्पर्धा और कमजोर कर दी है। झींगा और अन्य समुद्री उत्पादों का निर्यात, जिसमें अमेरिका सबसे बड़ा खरीदार रहा है, गहरे संकट में है। रोजगार के मोर्चे पर लाखों मज़दूर या तो बेरोज़गार हो सकते हैं या फिर अस्थिर आय पर काम करने को मजबूर होंगे।
अर्थशास्त्रियों का आकलन है कि यदि यह स्थिति लंबी चली तो भारत की विकास दर पर 0.4 से 0.5 प्रतिशत तक नकारात्मक असर पड़ सकता है। साथ ही अमेरिकी बाज़ार में भारत की जगह लेने के लिए वियतनाम, बांग्लादेश और मैक्सिको जैसे देश सक्रिय हो चुके हैं। वियतनाम पहले ही अमेरिका का पसंदीदा परिधान और फर्नीचर आपूर्तिकर्ता बन रहा है, जबकि बांग्लादेश का वस्त्र उद्योग सस्ते श्रम और कम लागत के चलते भारत से आगे निकलता दिख रहा है। अगर भारत ने समय रहते लॉजिस्टिक लागत, कर ढांचा और निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं को सरल नहीं किया, तो यह अवसर स्थायी रूप से अन्य देशों के हाथ में जा सकता है।
टैरिफ युद्ध का दूसरा आयाम भू-राजनीति है। अमेरिकी कदम सिर्फ व्यापार विवाद नहीं, बल्कि रूस के साथ भारत की बढ़ती नज़दीकी पर सीधी प्रतिक्रिया है। S-400 मिसाइल सिस्टम और ऊर्जा समझौतों पर अमेरिका की असहमति पहले ही खुलकर सामने आ चुकी है। साथ ही, अमेरिकी राजनीति में संरक्षणवाद अब चुनावी हथकंडा बन चुका है। ट्रंप अपने घरेलू वोट बैंक को साधने के लिए टैरिफ का इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे इसकी वैश्विक कीमत कुछ भी क्यों न हो।
यह भी ध्यान रखना होगा कि टैरिफ का नुकसान सिर्फ भारत को नहीं, अमेरिका को भी होगा। भारत पहले ही अमेरिकी बादाम, अखरोट और सेब पर जवाबी टैरिफ लगा चुका है, जिससे अमेरिकी किसानों की लॉबी को चोट पहुंची थी। अब नए टैरिफ उपभोक्ताओं के लिए महंगाई बढ़ाएंगे और अमेरिकी कंपनियों की लागत भी बढ़ेगी।
हालांकि यह संकट गहरा है, मगर भारत के पास विकल्प मौजूद हैं। यूरोपीय संघ, ब्रिटेन और ASEAN जैसे बाजारों में भारत अपने निर्यात को मज़बूत बना सकता है। इसके अलावा, बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ “चाइना+1” रणनीति के तहत चीन पर निर्भरता कम कर रही हैं। अगर भारत भूमि स्वीकृति, कानूनी प्रक्रियाओं और टैरिफ व्यवस्था को सरल बनाता है, तो वह वैश्विक निवेश का स्वाभाविक केंद्र बन सकता है। यही नहीं, इस झटके को अवसर में बदलने के लिए भारत को व्यापार विविधीकरण, कारोबारी माहौल सुधार और मानव संसाधन के बेहतर उपयोग पर फोकस करना होगा।
प्रोफेसर पारस नाथ चौधरी जैसे जानकारों का मानना है कि ट्रंप की टैरिफ नीति भारत के लिए तत्काल संकट है, लेकिन दीर्घकालिक नज़रिए से यह अवसर भी बन सकती है। सवाल यह नहीं है कि अमेरिका ने भारत के लिए दरवाज़ा बंद किया है, बल्कि यह है कि भारत कितनी जल्दी नए दरवाज़े खोलने की चाबी तलाश पाता है। संकट के इस दौर में वही राष्ट्र मज़बूत होकर उभरेगा, जो अपनी चुनौतियों को अवसर में बदलने का साहस रखता है।