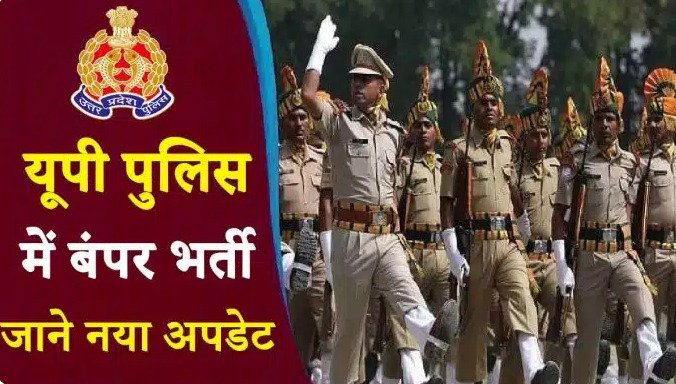इनकम टैक्स में 12 लाख तक की छूट का ऐसा प्रचार हो रहा है जैसे समाजवाद का सपना साकार हो गया हो। भारत की कुल आबादी में कितने प्रतिशत लोग सालाना 12 लाख रुपए कमाते हैं? मेट्रोज के बाहर, कितने पत्रकार हैं जो एक लाख रुपए महीने की सैलरी उठाते हैं? लेकिन आर्थिक क्रांति के ध्वजवाहक बने हुए हैं!
बृज खंडेलवाल
1 फरवरी को पेश किया गया केंद्रीय बजट 2025, सरकार की सवालिया प्राथमिकताओं को स्पष्ट रूप से उजागर करता है। इस बजट में करोड़ों “हाशिए के नागरिकों” की सामाजिक-आर्थिक समस्याओं को नजरअंदाज करते हुए संपन्न वर्गों का पक्ष लिया गया है। जबकि सरकार ने आयकर सीमा को ₹12 लाख तक बढ़ाकर बड़े वर्गों को राहत देने का दावा किया, यह कदम केवल उच्च आय वर्ग को लाभ पहुंचाने वाला प्रतीत होता है।
हाशिए पर खड़ी आम जनता की अनदेखी
कॉलेज टीचर राम निवास ने कहा, “हमें बजट ज्यादा समझ नहीं आता, लेकिन ऐसा लगता है कि यह बड़े लोगों के हितों को प्राथमिकता देकर, संपन्न वर्गों को कर लाभ प्रदान करता है और बेरोजगारी, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को दरकिनार कर मौजूदा असमानताओं को और मजबूत करता है।
होम मेकर पद्मिनी ने अपनी बात रखते हुए कहा, “सड़क छाप लोगों से बातचीत करने पर पता लगा कि भारत की बड़ी आबादी टैक्स सिस्टम के हाशिए से बाहर है, यानी औपचारिक वित्त व्यवस्था का हिस्सा नहीं है और उन्हें बजट से कोई खास फर्क नहीं पड़ता।”
बेरोजगारी और कम वेतन: सरकार की नाकामी
समाजवादी विचारक राम किशोर ने बजट पर टिप्पणी करते हुए कहा, “लाखों युवा भारतीयों के बेरोजगार या कम रोजगार वाले होने के कारण रोजगार सृजन, कौशल विकास और उचित वेतन की नीतियों की तत्काल आवश्यकता थी, लेकिन बजट इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाता।”
संपन्न वर्ग को फायदा, आम नागरिक की स्थिति में कोई बदलाव नहीं
वहीं, सरकार ने कर राहत उपायों को प्राथमिकता दी है और आयकर सीमा को बढ़ाकर ₹12 लाख कर दिया है। हालांकि, यह कदम केवल मध्यम और उच्च वर्ग को लाभ पहुँचाता है। कामकाजी वर्ग पहले ही मुद्रास्फीति और स्थिर मजदूरी के कारण अपनी क्रय शक्ति खो चुका है। इसके बावजूद, बजट ने विकास के ऐसे मॉडल पर ध्यान केंद्रित किया है जो मानता है कि लाभ “नीचे की ओर जाएगा”, लेकिन यह दृष्टिकोण पहले ही भारत समेत अन्य देशों में विफल हो चुका है।
स्वास्थ्य और शिक्षा: सुधार की आवश्यकता
सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए बजट का आवंटन अपर्याप्त है। प्रोफेसर पारस नाथ चौधरी ने कहा, “भारत के सार्वजनिक स्वास्थ्य ढांचे को तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है, लेकिन सरकारी अस्पतालों के विस्तार और मजबूती की बजाय, धन निजीकरण की ओर मुड़ रहा है, जिससे गरीबों को महंगी निजी चिकित्सा सेवाओं पर निर्भर होना पड़ता है।”
शिक्षा में भी स्थिति सुधरने का नाम नहीं ले रही। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा में निवेश की कमी के कारण भारत का भविष्य कार्यबल कमजोर बना हुआ है, जिससे सामाजिक-आर्थिक विभाजन गहरा होता जा रहा है।
कॉर्पोरेट लाभ की प्राथमिकता
सरकार ने कर रियायतों पर ध्यान केंद्रित किया है, जो उच्च आय वर्गों के लिए लाभकारी हैं। इस कदम से सरकार की पूंजीवादी एजेंडे के प्रति प्रतिबद्धता स्पष्ट होती है, जिसमें सार्वजनिक कल्याण की बजाय कॉर्पोरेट मुनाफे को प्राथमिकता दी जा रही है। इसके साथ ही, जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय स्थिरता के मुद्दे भी बजट में अनदेखे रहे, और नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश की बजाय बड़े उद्योगों को लाभ पहुँचाने का काम किया गया।
युवाओं की अनदेखी और असमानता में वृद्धि
भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन लगभग खत्म हो चुका है, लेकिन यह नहीं समझा जा सकता कि मजदूरों की स्थिति में सुधार हुआ है। यह भी संभव है कि मुफ्त अनाज और रेवड़ी वितरण की योजना से जनमानस में आक्रोश और विरोध की भावनाएँ दबाई जा रही हैं। आज की युवा पीढ़ी समाज को बदलने के सपने नहीं देखती, बल्कि अपनी लाइफस्टाइल और व्यक्तिगत हितों को सुरक्षित रखने में अधिक रुचि रखती है।
सच्चे आर्थिक न्याय की आवश्यकता
भारत को सच्चा आर्थिक न्याय प्राप्त करने के लिए ध्यान कॉर्पोरेट हितों से हटाकर मानव पूंजी पर केंद्रित करना चाहिए। अमीर और गरीब के बीच बढ़ती खाई को पाटने के लिए संरचनात्मक सुधार, प्रगतिशील कराधान और मजबूत सामाजिक कल्याण नीतियाँ आवश्यक हैं। तब तक, एक समतावादी समाज का सपना पहुंच से बाहर रहेगा, और लाखों लोग संघर्ष करते रहेंगे जबकि कुछ विशेषाधिकार प्राप्त लोग लाभ उठाएंगे।